Dr. BR Ambedkar Biography | Books | Lifestyle | Age | Social Reforms | Family Life & More
“इस पूरी दुनिया में गरीब वही है, जो शिक्षित नहीं है।
~ Dr. Br Ambedkar
इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना।”
दोस्तों, इस ब्लॉग में आप बाबासाहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के संघर्षों ( Dr. BR Ambedkar Biography In Hindi ) के बारे में पढ़ने वाले हैं। डॉ अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। लोग उन्हें प्यार से बाबासाहेब कहते थे। अम्बेडकर उनके गांव का नाम था, जिसे उन्होंने अपने एक शिक्षक की सलाह पर अपने नाम के पीछे जोड़ दिया था।
Bharat Ratna Baba Saheb Dr. BR Ambedkar Biography In Hindi
आपको डॉ. आंबेडकर की यह बायोग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए ?
दोस्तों, अगर आप जीवन की छोटी-छोटी मुश्किलों से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं तो आपको यह Dr. BR Ambedkar Biography In Hindi जरूर पढ़नी चाहिए। यह जीवनी एक ऐसे महान शख्स के बारे में है जिन्होंने सारी उम्र दुख तकलीफें सही, बचपन में सामाजिक भेदभाव की पीड़ा को झेला और जवानी में पत्नी व बच्चों की असामयिक मौत का दुख सहा, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और भारतीय इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ी जो सदियों तक भी अमिट रहेगी।
दोस्तों, हमें यह तो बताया जाता है की क्रिकेट खेलने वाले एक सोलह साल के लड़के सच्चिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रचा, बस में टिकट बेचने वाला रजनीकांत फ़िल्मी दुनिया का भगवान बना और पैसे न होने की वज़ह से बाहर बैंच पर सोने वाला शाहरुख़ खान बॉलीवुड की दुनिया का सुपरस्टार बना। लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता की कक्षा के बाहर बैठ कर पढ़ने वाले एक दलित ने भारत का संविधान लिखा और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह की वे पूरी दुनिया में ‘सिंबल ऑफ़ नॉलेज‘ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए।
बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे ? Who was Dr. BR. Ambedkar?

बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर ( Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar ) बीसवीं सदी के एक महान विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित और बौद्ध विचारधारा से प्रेरित होकर दलितों के अधिकारों के लिए और उनके साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके अलावा वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष, ब्रिटिश भारत में वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे।
डॉ अम्बेडकर एक विशिष्ट प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी।
डॉ अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था ? | Birth of Dr. Ambedkar
डॉ भीमराव अम्बेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत में 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत ( वर्तमान में मध्य प्रदेश ) के महू में एक सैन्य छावनी में हुआ था। इनके पिता श्री रामजी मालोजी सकपाल अंग्रेजी सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। अम्बेडकर, इनके पिता रामजी मलोजी सकपाल और माता श्रीमती भीमाबाई सकपाल की 14वीं और आखिरी संतान थे। इनका परिवार अब के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे शहर से एक मराठी पृष्ठभूमि से संबंध रखता था। डॉ अम्बेडकर के पुरखों ने काफी लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए काम किया था।
डॉ अम्बेडकर का प्रारंभिक जीवन कैसा था ? Dr. Ambedkar’s Early Life
डॉ भीमराव अम्बेडकर ने बचपन के शुरुआती दिनों से ही सामाजिक भेदभाव की पीड़ा को सहा था। जब बचपन में वे स्कूल जाते थे तो अम्बेडकर व अन्य दलित बच्चों को अलग-थलग, कमरे से बाहर बैठाया जाता था। शिक्षकों द्वारा भी उन पर कम ध्यान दिया जाता था। उन्हें कक्षा से बाहर एक बोरी पर बैठना पड़ता था, जिसे वे अपने साथ लाते थे। स्कूल के दौरान जब उन्हें कभी प्यास लगती तो वह खुद से घड़े से पानी लेकर भी नहीं पी सकते थे।
प्यास लगने पर वह पानी के घड़े के थोड़ी दूर खड़े हो जाया करते थे ( क्योंकि छोटी जाति का होने की वजह से उन्हें घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी ) इसके बाद अगर कोई उच्च जाति का बच्चा पानी पीने के लिए आता या फिर चपरासी की नजर उस पर पड़ जाती, तभी उन्हें पानी मिल पाता था। कभी-कभी तो उन्हें पानी मिलने की आस में घंटों पानी के घड़े के पास खड़े रहना पड़ता और बिना पानी पिए ही वापस लौटना पड़ता।
जब पानी मिलता भी था तो उसकी भी कुछ विशेष शर्तें होती थी। पानी पिलाने वाला लगभग 1 फुट ऊपर से पानी डालता था, तब उन्हें पानी पीना पड़ता था। डॉ अम्बेडकर द्वारा लिखी उनकी आत्मकथा ‘वेटिंग फॉर ए वीजा‘ में उन्होंने इस स्थिति का वर्णन भी किया है जिसे उन्होने “नो चपरासी, नो वाटर” के रूप में वर्णित किया है।
बाबा साहेब आंबेडकर के माता पिता कौन थे ? Dr. Ambedkar’s Parents
अम्बेडकर अपने पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता श्रीमती भीमाबाई सकपाल की 14वीं और अंतिम संतान थे। रामजी सकपाल के 14 बच्चों में से केवल 5 बच्चे ही जीवित थे जिनमें से तीन बेटे थे बलराम, आनंद राव व सबसे छोटे भीम राव और दो बेटियां थी मंजुला और तुलासा। अपने पांचों भाई बहनों में डॉ अम्बेडकर ही ऐसे थे जो स्कूल जाते थे।
1894 में डॉ भीमराव अम्बेडकर जी के पिता श्री रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए और 2 साल बाद ही उनका पूरा परिवार सतारा, महाराष्ट्र चला गया। यहां आने के कुछ वर्षों बाद ही जब अम्बेडकर की उम्र केवल 7–8 साल थी, उनकी मां भीमाबाई का निधन हो गया। इस तरह से बहुत छोटी सी उम्र में ही अम्बेडकर के सिर से मां का साया उठ गया था। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी बुआ मीराबाई ने की। इस तरह से बड़ी कठिन परिस्थितियों में अम्बेडकर का बचपन गुजरा।
भीमराव का नाम भीमराव अम्बेडकर कैसे पड़ा ?
हालांकि बचपन में अपने पिता श्री रामजी सकपाल के नाम के आधार पर उनका नाम भीमराव सकपाल था। लेकिन इनके पिता ने स्कूल में इनका नाम इनके पैतृक गांव अंबाडावे के नाम पर भीमराव अंबाडावेकर लिखवाया। लेकिन उनके एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण जी केशव अम्बेडकर ( एक देवरूखे ब्राह्मण, महाराष्ट्र की ब्राह्मणों की पांच उप जातियों में से एक ) ने स्कूल के रिकॉर्ड में इनका उपनाम अंबाडावेकर से बदलकर अम्बेडकर कर दिया।
डॉ अम्बेडकर जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी ? Dr. Ambedkar’s Primary Education
डॉ भीमराव अम्बेडकर की आरंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में ही हुई। बाद में 1897 में जब इनका पूरा परिवार सातारा छोड़कर मुंबई चला गया तो वहां अम्बेडकर जी ने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले लिया, जहां से 1907 में अम्बेडकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। डॉ अम्बेडकर एलफिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले पहले व एकमात्र दलित छात्र थे।
डॉ अम्बेडकर जी का विवाह कब हुआ था ? Dr. Ambedkar’s Married Life
1906 में जब डॉ भीमराव अम्बेडकर की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी और वह नौवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उनका विवाह एक 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से हो गया। उस समय प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार अम्बेडकर जी का विवाह हुआ।
डॉ अम्बेडकर जी की उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी ? Dr. Ambedkar’s High Education

1. मुंबई विश्वविद्यालय से पोस्ट मेट्रिक ।
1907 में एलफिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉ अम्बेडकर जी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त एलफिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया। ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति थे जो एक अछूत जाति से संबंधित होने के बावजूद कॉलेज गए थे। इस उपलक्ष में समुदाय के लोगों द्वारा उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया, जहां उन्हें उनके पारिवारिक मित्र व प्रबुद्ध लेखक दादा केलुसकर द्वारा बुध की जीवनी भेंट की गई थी।
2. कोलंबिया विश्वविद्यालय से मास्टर इन इकोनॉमिक्स।
1913 में जब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी केवल 22 साल के थे, बड़ौदा रियासत के राजा सयाजीराव गायकवाड तृतीय के द्वारा चलाई जा रही एक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अम्बेडकर जी को सम्मानित किया गया था, जिसके तहत किसी भी होनहार बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बड़ौदा रियासत द्वारा प्रतिमाह 11.50 स्टर्लिंग ( 3 साल तक ) स्कॉलरशिप के रूप में आर्थिक सहायता दी जानी थी।
हालाँकि आर्थिक सहायता के एवज में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा रियासत में 5 साल तक नौकरी करनी पड़ती। अमेरिका आने के बाद यहां डॉ भीमराव अम्बेडकर जी की मुलाकात एक पारसी विद्यार्थी नवल भयेना से हुई। यहां लिविंगस्टन हॉल में ये उनके साथ रहते थे और बाद में ये आजीवन डॉ अम्बेडकर के दोस्त भी रहे।
जून 1915 में डॉ भीमराव अम्बेडकर जी ने अर्थशास्त्र में अपने M.A की परीक्षा उत्तीर्ण की। अर्थशास्त्र के साथ-साथ वे समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और नृवविज्ञान आदि विषयों में भी गहरी रूचि लेते थे और इन विषयों के बारे में भी लाइब्रेरी में गहन अध्ययन करते थे। M.A के लिए उनकी थिसिस थी ‘प्राचीन भारतीय वाणिज्य’
अम्बेडकर जी जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1916 में उन्होंने दोबारा M.A की और दूसरी थीसिस लिखी जिसका विषय था ‘नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया: ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी’
9 मई 1916 को उन्होंने एक एंथ्रोपॉलजिस्ट एलेग्जेंडर गोल्डनवाइजर द्वारा आयोजित सेमिनार से पहले एक पेपर प्रस्तुत किया जिसका विषय था ‘कास्ट इन इंडिया :देअर मेकैनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट‘
3. लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी से M.A करने के बाद वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने अक्टूबर 1916 में Gray’s Inn के बार कोर्स में दाखिला लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। यहां उन्होंने डॉक्टरेट थीसिस पर काम शुरू किया। लेकिन जून 1917 में उन्हें इस वजह से भारत लौटना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा रियासत की तरफ से मिलने वाली छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो चुकी थी।
लंदन से भारत वापसी में उनके साथ कौन सी दुखद घटना घटी ?
कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के दौरान उन्होंने अपनी रूचि और अध्ययन विषयों से संबंधित बहुत सी किताबों का संग्रह किया था। उनके इस पुस्तक संग्रह को उस जहाज की बजाए ( जिस जहाज से वह लंदन से भारत आ रहे थे ) किसी दूसरे जहाज से भेजा गया था। लेकिन वह जहाज रास्ते में ही एक जर्मन पनडुब्बी के तारपीडो के हमले द्वारा समुंदर में डुबो दिया गया ( प्रथम विश्व युद्ध के कारण )। जब इस घटना के बारे में अम्बेडकर जी को पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। यह दुनिया के बेहतरीन लेखकों द्वारा लिखी पुस्तके उन्होंने बड़ी मुश्किलों से जमा की थी।
भारत लौटने के बाद बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार उन्हें वहां नौकरी करनी पड़ी। यहां उन्हें बड़ौदा सेना के सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन वे यहां केवल 11 दिन तक ही नौकरी कर पाए और 11 दिन बाद उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘वेटिंग फॉर ए विजा’ में इस घटना का वर्णन किया है।
बड़ौदा रियासत में नौकरी के वे 11 दिन कैसे बीते ?
इस घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है कि जब वे वहां गए तो उन्हें अछूत होने की वजह से रहने के लिए कहीं भी कमरा नहीं मिला। वह कई हिंदू होटलों और धर्मशालाओं में गए, लेकिन हर जगह से उन्हें अछूत होने की वजह से मना कर दिया जाता था। आखिर में वह एक पारसी सराय में पहुंचे, जहां उन्हें रहने के एवज में ज्यादा पैसे देने और क्योंकि वहां गैर पारसियों को रहने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए पारसी नाम रजिस्टर में दर्ज करवाने पर रहने की अनुमति मिली। डॉ अम्बेडकर मजबूरी वश ज्यादा पैसे देने और पारसी नाम रखने के लिए राजी होना पड़ा।
लेकिन कुछ दिनों बाद जब वहां के पारसी लोगों को बाबा साहेब की असलियत का पता चला की वे पारसी नहीं बल्कि छोटी जाति से संबंध रखने वाले एक दलित है तो 15–20 पारसियों की गुस्साई भीड़ लाठी-डंडे लेकर सुबह सुबह ही सराय में पहुंच गई। इस गुस्साई भीड़ ने बाबा साहेब को बहुत बुरा भला कहा, जातिवादी गालियां दी और शाम तक सराय छोड़कर चले जाने को कहा। बाबा साहब को उसी दिन वह पारसी सराय छोड़नी पड़ी। रहने के लिए कोई ठिकाना ना होने की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और वापस मुंबई लौटना पड़ा।
यहां के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है कि ऑफिस में भी कोई उनसे बात नहीं करता था। क्योंकि ऑफिस के सभी कर्मचारी ऊंची जाति के थे। वहां का चपरासी भी फाइलों को एक डंडे से बांधकर उनके टेबल पर पटक देता था। जब डॉ अम्बेडकर वहां चपरासी से पीने के लिए पानी मांगते तो वह मना कर देता और कहता था कि पीने के लिए पानी अपने घर से लेकर आओ। अगर बाबा साहेब किसी वस्तु को छू देते तो उसे गोमूत्र से धोया जाता। यहां तक कि जब काम होने के बाद चपरासी फाइलों को वापस लेकर जाता था तो उन पर भी गोमूत्र से छिड़काव करता था।
इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार के कारण डॉ अम्बेडकर को यहां नौकरी करना मुश्किल हो गया था और जब उन्हें पारसी सराय से निकाला गया तो वे पूरी तरह से टूट चुके थे। सराय छोड़ने के बाद जब वे मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गए तो ट्रेन आने में अभी समय था। इसलिए वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए।
डॉ अम्बेडकर को ऐसा कब लगा की उनको दलित समाज के बारे में कुछ करना चाहिए ?
बड़ौदा रियासत में नौकरी करने के अपने अनुभव बारे में लिखते हुए डॉ अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है कि “यहां मैने पहली बार यह सीखा था कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है यानी अस्पृश्यता की यह बुराई पूरे समाज में फैली हुई है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर मेरे साथ यह भेदभाव हो रहा है, तो मेरे जैसे लाखों अछूत हैं जो इस तरह की भेदभाव पूर्ण जिंदगी जीने के लिए मजबूर होंगे। उनके साथ क्या होता होगा। यही से पहली बार बाबासाहेब ने पिछड़ों व अछूतों के लिए कुछ करने और उनकी सामाजिक भेदभाव की बेड़ियों को काटने का संकल्प लिया था।
बड़ौदा से मुंबई लौटने के बाद वे एक निजी ट्यूटर व लेखाकार के रूप में काम करने लगे। उन्होंने कुछ समय के लिए वित्तीय परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति के कारण वे इसमें भी विफल रहे। इसके बाद उनके एक अंग्रेज मित्र मुंबई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड सेडनम के कारण उन्हें मुंबई के सेडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई।
लंदन की उनकी दोबारा यात्रा कैसे संभव हो पायी ?
डॉ अम्बेडकर को 4 साल के भीतर अपनी थीसिस जमा करने के लिए अनुमति मिली थी। लेकिन उनके पास दोबारा लंदन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। जब यह बात कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज को पता चली तो वे आर्थिक मदद के लिए आगे आए।
कोल्हापुर रियासत के राजा और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर रियासत की बागडोर 1894 में संभाली थी। साहू जी महाराज ने डॉ अम्बेडकर समेत हर उस राजनेता और समाज सुधारक की नैतिक और आर्थिक मदद की जो उस समय सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनके द्वारा की गई आर्थिक मदद की बदौलत ही डॉ अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दोबारा लंदन जा सके।
डॉ अंबेडकर शिक्षा को इतना महत्व क्यों देते हैं ?
डॉ भीमराव अम्बेडकर में पढ़ने की इतनी ललक थी कि वह लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन से पहले पहुंच जाया करते थे और रात को जब लाइब्रेरी बंद होती थी तभी लौटते थे। लाइब्रेरियन भी उनको जानने लगे थे। लाइब्रेरी से लौटने के बाद भी वे रात को घंटों तक पढ़ते रहते थे। डॉ अम्बेडकर मानते थे कि शिक्षा ही वह एकमात्र हथियार है जिसकी वजह से दलित और अछूत समाज की गुलामी की बेड़ियों को काटा जा सकता है। वह कहते थे कि ’शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पियेगा वही दहाड़ेगा’ ।
गरीबी के कारण डॉ अम्बेडकर महंगी किताबें खरीद पाने में असमर्थ थे, इसलिए वे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा किताबें लाइब्रेरी से ही पढ़ ली जाए।
लंदन में साहू जी महाराज ने डॉ आंबेडकर की सहायता कैसे की ?
डॉ अम्बेडकर की लंदन की पढ़ाई के दौरान कोहलापुर रियासत के राजा साहू जी महाराज ने उनकी काफी मदद की। जब लंदन में डॉ अम्बेडकर पैसे की कमी से जूझ रहे थे और उनके पास खाने-पीने, फीस भरने और भारत वापस आने तक के पैसे नहीं थे।
तो उन्होंने 4 सितंबर 1921 को आर्थिक मदद के लिए साहू जी महाराज को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में लिखते हुए कहा कि “महाराज! में अपनी वित्तीय स्थिति इस आशा के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि कुछ मदद मिलेगी। महाराज! मुझे 100 पाउंड अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए व 100 पाउंड भारत वापस आने के लिए चाहिए। मैं महाराज का बहुत आभारी रहूंगा। अगर महाराज लोन के रूप में ही सही 200 पाउंड की व्यवस्था मेरे लिए कर दें, लंदन से वापस आने के बाद में महाराज का यह लोन ब्याज सहित वापस करूंगा।”
ऐसी कठिन परिस्थितियों में साहू जी महाराज ने ना केवल लंदन में डॉ अम्बेडकर को मदद पहुंचाई। बल्कि भारत में भी उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर को वित्तीय मदद भिजवाई।
लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की ?

1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से मास्टर की डिग्री हासिल की। उनकी थिसिस “रुपए की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान” पर थी।
साल 1923 में डॉ भीमराव अम्बेडकर जी ने लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में D.Sc की डिग्री हासिल की और उसी साल उन्होंने Gray’s Inn की तरफ से भी बैरिस्टर एट लाज डिग्री से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया।
लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटने के दौरान बहुत कम समय ( लगभग 3 महीने ) वे जर्मनी में भी रहे। वहां उन्होंने जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। लेकिन पैसे की कमी के कारण उन्हें जल्द ही भारत वापस लौटना पड़ा।
Note -: डॉ अम्बेडकर ने अपनी तीसरी डॉक्टरेट की उपाधि LLD 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हासिल की और 1953 में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
डॉ अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष कब शुरू किया ?
डॉ भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत की पीड़ा को झेला था, वह कहते थे “छुआछात गुलामी से भी बदतर है” अछूत होने के कारण बचपन से लेकर अब तक उन्होंने कई बार छुआछात का अपमान सहा था।
चाहे यह 1901 की घटना हो जब अम्बेडकर केवल 10 साल के थे और अपने भाई बहनों के साथ अपने पिता से मिलने के लिए सतारा से कोरेगांव जा रहे थे। उन्होंने इस घटना का वर्णन अपनी आत्मकथा ‘वेटिंग फॉर ए विजा’ में भी किया है। तब उन्होंने पहली बार छुआछूत का असली रूप देखा था। कोई बैलगाड़ी वाला भी उनको बैठाने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि वह दुगने पैसे देने को भी तैयार थे।
चाहे वह उनके स्कूल के दौरान पानी के लिए जातिगत भेदभाव की घटना हो या फिर बड़ौदा रियासत में नौकरी के लिए रहने की जगह ना मिलने की घटना। डॉ अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत की पीड़ा का व्यक्तिगत रुप से सामना किया था। इसलिए लंदन से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वे अछूतों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निम्न प्रयास किए
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 जिसे साउथबरो समिति तैयार कर रही थी, ने डॉ अम्बेडकर को एक प्रमुख विद्वान के रूप में उनके सुझाव जानने के लिए आमंत्रित किया था। इस सुनवाई के दौरान डॉ भीमराव अम्बेडकर ने दलितों व अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल बनाने व अछूतों व पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण देने की वकालत की थी।
- अछूतों व पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए 1920 में कोल्हापुर रियासत के महाराजा साहू जी महाराज की मदद से उन्होंने मुंबई में एक साप्ताहिक अखबार मूकनायक का प्रकाशन आरंभ किया।
- 1926 में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने एक कानूनी पेशेवर के रूप में काम करते हुए 3 गैर ब्राह्मण नेताओं को कोर्ट से बरी करवाया था। जिन्होंने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया था। इस जीत के बारे में एक पत्र में लिखते हुए धनंजय कीर ने लिखा कि “यह जीत ग्राहकों व डॉक्टरों के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से शानदार थी।”
- मुंबई उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करते हुए उन्होंने दलितों में शिक्षा को बढ़ावा देने और उनका सामाजिक व राजनीतिक उत्थान करने का प्रयास किया।
- उनका प्रथम संगठित प्रयास केंद्रीय संस्था ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ की स्थापना के रूप में था, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में अछूतों की कठिनाइयों को दूर करने, उनकी शिकायतों को सरकार के समक्ष रखने व अछूतों में एक नई सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए की गई थी।
- इसके अलावा उन्होंने दलितों व पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत व जनता आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया।
साइमन कमिशन के सन्दर्भ में डॉ अम्बेडकर की क्या भूमिका रही ? Dr. Ambedkar & Simon Commission
1925 में डॉ भीमराव अम्बेडकर को साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी कमेटी में नियुक्त किया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के संवैधानिक सुधारों की जांच करने और भारत के लिए और अधिक सुधारों का सुझाव देने के लिए 10 साल बाद एक आयोग भारत भेजा जाएगा। इसी आयोग को साइमन कमीशन के रूप में जाना जाता है।
नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट बनाने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया। इसकी अध्यक्षता सर साइमन ने की थी। यह कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था। भारतीयों ने इस कमीशन का कड़ा विरोध किया था। क्योंकि इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। हालांकि डॉ अम्बेडकर व पेरियार ई वी रामास्वामी ने इस आयोग का समर्थन किया था।
साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करने व प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा इसने पृथक निर्वाचन मंडल बनाए रखने की भी सिफारिश की और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल के जो अधिकार केवल मुसलमानों व निम्न जातियों को दिए गए थे, उनका विस्तार करते हुए दलितों को भी दे दिया गया। जिसका बाद में कड़ा विरोध किया गया। यह बाबा साहब के प्रयासों का ही नतीजा था।
Note -: डॉ भीमराव अम्बेडकर ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन में होने वाले तीनो गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया।
पूना पैक्ट के सन्दर्भ में डॉ अम्बेडकर की भूमिका क्या थी ? Dr. Ambedkar & Poona Pact
1932 में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने ‘कम्युनल अवार्ड’ के रूप में दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के गठन की घोषणा की। एक अलग निर्वाचक मंडल से यह अभिप्राय था कि कुछ निश्चित निर्वाचित सीटों पर दलित प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते थे।
लेकिन महात्मा गांधी ने दलितों के लिए इस तरह के निर्वाचक मंडल का कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार इस तरह की व्यवस्था से हिंदू समाज कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में कैद थे। वहीं से उन्होंने निर्वाचक मंडल का विरोध शुरू कर दिया और आमरण अनशन पर बैठ गए। कई दिनों के उपवास के कारण जब गांधी जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो डॉ अम्बेडकर ने मजबूर होकर गांधी जी से मिलने का फैसला किया।
25 सितंबर 1932 में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मदन मोहन मालवीय और पलवंकर बालू ने यरवदा जेल में डॉ अम्बेडकर के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की और उसी दिन एक समझौते के रूप में पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिंदुओं में दलित वर्गों की ओर से डॉ अम्बेडकर ने और अन्य हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के बाद दलितों को मिली 71 आरक्षित सीटों को बढ़ाकर 148 ही कर दिया गया, जैसा कि प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के तहत भारतीय सरकार द्वारा पहले प्रस्तावित सांप्रदायिक पुरस्कार में आवंटित किया गया था। इस पैक्ट में हिंदुओं के बीच अछूतों को निरूपित करने के लिए ‘डिप्रेस्ड क्लासेस’ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जिसे बाद में 1935 के भारत सरकार अधिनियम और 1950 में भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कहा गया। इस तरह अछूतों के लिए बाबा साहब डॉ अम्बेडकर द्वारा किया यह कार्य बहुत ही सराहनीय है।
बाद में भारतीय संविधान में भी पूना पैक्ट कि इन प्रस्तावों को शामिल कर लिया गया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित कर दी गई, जिन सीटों पर केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं।
डॉ आंबेडकर द्वारा किये गए अन्य सामाजिक आंदोलन क्या थे ?
1. महाड सत्याग्रह 1927 ( Mahad Satyagraha 1927 )
1927 में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों को सामाजिक अधिकार दिलाने व अस्पृश्यता के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया। उस समय अछूतों को बड़ी ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन करना पड़ता था। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक किसी भी रूप से उन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिले हुए थे। उन्हें छोटी-छोटी गंदी झोपड़ियों में रहना पड़ता था। उनके घर, गांव से बाहर होते थे। उन्हें सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं था।
लोगों का मानना था कि वह जिस चीज को छू लेंगे वह अपवित्र हो जाएगी। उन्हें कमर में झाड़ू बांधनी पढ़ती थी, ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर नाम पड़े। क्योंकि ब्राह्मण मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अछूतों के पद चिन्हों पर पांव रख देता तो अगले जन्म में अछूत पैदा होता।
इसके अलावा उन्हें गले में छोटी हंडिया लटका कर चलना पड़ता था। गले में पड़ी यह हंडिया उनके थूकने के लिए होती थी, ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र ना हो जाए। उन्हें केवल दोपहर के समय बाहर निकलने की अनुमति होती थी। क्योंकि दोपहर में सूर्य बिल्कुल सीधे सिर पर होने के कारण उनकी छाया किसी दूसरे व्यक्ति पर ना पड़े और वह अपवित्र ना हो जाए।
उन्हें बाहर निकलते वक्त कोई बर्तन और उसे बजाने के लिए एक डंडा रखना पड़ता था। वे उस बर्तन को बजाते हुए चलते थे ताकि सामने वाले व्यक्ति को दूर से ही पता चल जाए की कोई अछूत आ रहा है और वह अपना बचाव कर सकें।
उन्हें कुए व तालाबों पर पानी पीने की अनुमति नहीं थी। उनके पानी के लिए अलग स्त्रोत होते थे। जहां आमतौर पर भैंस, कुत्ते व अन्य जानवर नहाते थे। उन्हें गांव में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मजबूरी वश मरे हुए जानवरों का मांस खाना पड़ता था। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और न ही उन्हें मंदिर जाने का अधिकार था।
डॉ भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में अछूतों को पीने के स्वच्छ पाने के अधिकार दिलाने के लिए सबसे पहला आंदोलन महाड के तालाब पर किया। जहां डॉ अम्बेडकर व हजारों दलितों ने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को सभी के लिए खोलने के लिए सार्वजनिक आंदोलन किया और मार्च निकाला। जहां हजारों की संख्या में अछूत महाड तालाब पर इकट्ठा हुए और पहली बार बाबासाहेब के नेतृत्व में स्वच्छ जल ग्रहण किया।
बाबासाहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर के अनुसार “हिंदू एक कुत्ते का छुआ पानी पी सकता है। लेकिन अछूत का छुआ पानी उनके लिए जहर के समान है।” इसलिए अछूतों की स्थिति समाज में कुत्ते से भी बदतर थी।
2. मनुस्मृति का दहन 1927 ( Combustion of Manu Smriti 1927 )
1927 के अंत में, एक सम्मेलन में डॉ भीमराव अम्बेडकर व कुछ अन्य दलित कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ, मनुस्मृति का दहन किया। उनके अनुसार इस धर्म ग्रंथ में अछूतों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से उचित ठहराया गया है। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृति की सार्वजनिक रूप से निंदा की और सार्वजनिक रूप से इस किताब की प्रतियों को जलाया गया। 25 सितंबर 1927 को डॉ अम्बेडकर व उनके हजारों अनुयायियों ने मनुस्मृति का दहन किया। इस कारण अम्बेडकरवादियों व दलितों द्वारा हर वर्ष 25 सितंबर को मनु स्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
3. काला राम मंदिर आंदोलन 1930 ( Kala Ram Mandir Movement 1930 )
लगभग 3 महीने की तैयारी के बाद डॉ भीमराव अम्बेडकर व उनके लगभग 15000 अनुयायियों ने नासिक के कालाराम मंदिर में एकत्र होकर आंदोलन किया। यह आंदोलन अछूतों द्वारा हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए संघर्ष की शुरुआत थी। देखते ही देखते आंदोलन नासिक के सबसे बड़े जुलूसों में से एक बन गया। इस जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड और स्काउट्स के एक बैच द्वारा किया जा रहा था।
यह पहली बार था कि भगवान के दर्शन के लिए दलित महिलाओं व पुरुषों की भीड़ उचित अनुशासन, व्यवस्था और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचने से पहले ही ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए। डॉ अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है।
उन्होंने मंदिर के अधिकारियों को भी समझाने की कोशिश की कि वे शांति पूर्वक भगवान के दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब उसके बाद भी मंदिर के द्वार नहीं खोले गए तो उन्हें अपने अनुयायियों के साथ वहीं से वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद ब्राह्मणों में एक डर पैदा हो गया था और वह डॉ अम्बेडकर के साहस और ज्ञान से डरने लगे थे।
4. खोटी व्यवस्था’ के खिलाफ लड़ाई 1937 ( Khoti System )
1937 में ही उन्होंने कोकण में प्रचलित एक शोषण व्यवस्था ‘खोटी व्यवस्था’ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस खोटी व्यवस्था के तहत खोट यानी सरकारी राजस्व संग्रहकर्ता, किसानों व काश्तकारों का नियमित तौर पर शोषण करते थे। 1937 में ही उन्होंने ‘खोटी व्यवस्था’ को खत्म करने वह सरकार व किसानों के बीच सीधा संबंध बनाने के उद्देश्य से मुंबई विधानसभा में एक विधेयक भी पेश किए।
डॉ अम्बेडकर का राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू हुआ ? Dr. Ambedkar’s Political Career
1935 में डॉ अम्बेडकर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने लगभग 2 साल तक कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के शासी निकाय में अध्यक्ष पद पर भी काम किया।
1936 में उन्होंने ‘इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी’ की स्थापना की, जिसने मुंबई के केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी की तरफ से 13 आरक्षित व 4 सामान्य सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे गए। जिनमें से उनकी पार्टी ने आरक्षित सीटों पर 11 में व सामान्य सीटों पर 03 में जीत हासिल की।
डॉ भीमराव अम्बेडकर ने 15 मई 1936 में अपनी पुस्तक ‘एनीहिलेशन ऑफ कास्ट’ प्रकाशित की जिसमें उन्होंने कुछ हिंदू धार्मिक रूढ़िवादी नेताओं को उनकी जातिवादी सोच के लिए और मुख्य रूप से जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की।
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य करते हुए उन्होंने क्या सुधार किये ? Dr. Ambedkar As A Labour Minister
अम्बेडकर ने जुलाई 1942 से अक्टूबर 1946 तक ब्रिटिश भारत की रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 8 नवंबर 1943 को डॉ अम्बेडकर द्वारा पेश किए गए ‘भारतीय ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक’ में उन्होंने मजदूरों व श्रमिकों के कल्याण के लिए कई प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए जैसे –
- लिंग की परवाह किए बिना समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। जिसकी वजह से महिलाओं को समान काम के बदले समान वेतन देने का प्रावधान किया गया।
- कारखानों में काम करने के घंटों को कम करना। पहले कारखानों में श्रमिकों को 14 घंटे काम करना पड़ता था लेकिन डॉ अम्बेडकर के प्रयासों से काम के घंटों में कमी करके उन्हें 8 घंटे किया गया।
- पहले कोयला खदानों में महिलाओं के कार्य करने पर प्रतिबंध था, इस अधिनियम में इस प्रतिबंध को हटाया गया।
- इस अधिनियम के लागू होने के बाद रोजगार कार्यालयों की स्थापना में मदद मिली। जिसकी वजह से ट्रेड यूनियनों, मजदूरों व सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से श्रम मुद्दों को निपटाने में मदद मिली।
- इसके अलावा इस अधिनियम में कर्मचारी राज्य बीमा, क्षतिपूर्ति बीमा के रूप में चिकित्सा देखभाल,चिकित्सा अवकाश, शारीरिक रूप से अक्षम श्रमिकों के लिए विशेष सुविधाएं व महिलाओं को मातृत्व लाभ देना आदि प्रावधान किए गए।
इस अधिनियम के अलावा भी डॉ अम्बेडकर ने श्रम मंत्री के रूप में कार्य करते हुए श्रमिकों, कर्मचारियों, महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए निम्न विधेयक पेश किए जैसे खान मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम आदि।
डॉ. आंबेडकर ने ‘शूद्र कौन थे’ किताब क्यों लिखी ? ‘Shudra Koun The’ Books By Dr. Ambedkar
1946 में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था शूद्र कौन थे। इस किताब में उन्होंने अछूतों के गठन की अवधारणा की व्याख्या करने की कोशिश की। इस किताब में उन्होंने बताया कि शूद्र और अति शूद्र अछूतों से अलग है और यह जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीचे आते हैं। उनकी यह पुस्तक शूद्रवर्ण की उत्पत्ति व जाति व्यवस्था के पदानुक्रम को प्रदर्शित करती है। डॉ अम्बेडकर ने अपनी इस पुस्तक को ज्योति राव फूले को समर्पित किया।
1946 से 1956 तक उनका राजनैतिक कैरियर कैसा रहा ?
1946 के भारतीय संविधान सभा के चुनाव में उनकी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया और वे चुनाव हार गए। लेकिन बाद में उन्हें बंगाल की तरफ से इस विधानसभा में चुना गया, जहाँ मुस्लिम लीग सत्ता में थी।
डॉ भीमराव अम्बेडकर ने 1952 में लड़े गए पहले भारतीय आम चुनाव में मुंबई नॉर्थ की तरफ से चुनाव लड़ा। लेकिन वे अपने पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजरोलकर से चुनाव हार गए।
लेकिन 1952 में ही उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1954 में उन्होंने लोकसभा में प्रवेश करने के लिए 1954 के उपचुनाव में भाग लिया। लेकिन वे दोबारा से भंडारा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से हार गए। उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु होने के कारण वे 1957 के आम चुनाव में भाग नहीं ले सके।
भारत के विभाजन के सन्दर्भ में डॉ अम्बेडकर की क्या भूमिका रही ?
1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग करने वाला ‘लाहौर प्रस्ताव’ पेश किया गया था। इसके बाद डॉ भीमराव अम्बेडकर ने 400 पेज का एक लेख लिखा। इसका विषय था ‘पाकिस्तान पर विचार’ इस लेख में उन्होंने आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक हर पहलू से पाकिस्तान की अवधारणा पर विचार किया और अंततः यह तर्क प्रस्तुत किया कि हिंदुओं को मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों दे देना चाहिए।
उनके इस लेख ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवाद का रास्ता निर्धारित किया और इस तरह पाकिस्तान के जन्म और भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
भारत के पहले क़ानून मंत्री के रूप में उनकी क्या भूमिका रही ? Dr. Ambedkar As First Law Minister Of India
15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों सालों की अंग्रेजी गुलामी से आजाद हो गया। नवराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी और इस नवनिर्मित सरकार में डॉ भीमराव अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनने और अपनी सेवाएं देने का मौका मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
इस नवनिर्मित राष्ट्र को एक समान रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। जिसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो राष्ट्र को एकीकृत, संगठित और विकसित होने में मदद करें और इसके नागरिकों को सामाजिक,आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता प्रदान करें।
संविधान सभा के सदस्यों को ( 389 सदस्य, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद इनकी संख्या 299 रह गई थी ) प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के तहत कुछ समितियां बनाई गई थी, जिनमें से संविधान मसौदा समिति मुख्य थी। क्योंकि इसका कार्य था संविधान के मुख्य भाग को तैयार करना। डॉ अम्बेडकर के ज्ञान और काबिलियत की वजह से उन्हें इस संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ अम्बेडकर का क्या योगदान था ? Dr. Ambedkar’s Role As An Architech Of Indian Constitution
डॉ भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस संविधान मसौदा समिति ने 11 सत्रों में ( लगभग 3 सालों में ) संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान की मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। हालांकि संविधान का मसौदा तैयार करने यानी संविधान के मुख्य भाग को तैयार करने में डॉ अम्बेडकर की अहम भूमिका रही।
संविधान का मसौदा तैयार होने के बाद जब इसे संविधान सभा को सौंपा गया तो संविधान की मसौदा समिति के एक सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान के निर्माण में डॉ अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन अपने भाषण में करते हुए कहा कि
“अध्यक्ष महोदय ! मैं सदन के उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने सदन के दौरान डॉ अम्बेडकर की बात को बहुत सावधानी से सुना है। मुझे इस बात की जानकारी है कि इन्होंने ( डॉ अम्बेडकर ने ) इस सविधान का मसौदा तैयार करने के काम में कितनी मेहनत और उत्साह से काम किया। साथ ही मुझे इस बात का भी पता है कि इस समय हमारे लिए इस महत्वपूर्ण संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जितने ध्यान की आवश्यकता थी, संविधान मसौदा समिति द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया गया।
सदन को शायद इस बात की जानकारी है कि संविधान मसौदा समिति के लिए आपके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक सदस्य ने सदन से त्यागपत्र दे दिया था, जिसे बदला नहीं गया। उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जगह किसी दूसरे सदस्य को नियुक्त नहीं किया गया। उनमें से एक अमेरिका में थे, उसका स्थान भी नहीं भरा गया और एक सदस्य राज्य के मामलों में व्यस्त थे। एक दो सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे और स्वास्थ्य कारणों से उन्हें आने नहीं दिया गया। तो अंततः ऐसा हुआ कि विधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉ अम्बेडकर कर पर आ गया। “
टीटी कृष्णमाचारी के इस भाषण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका रही। इसलिए उन्हें ‘भारतीय संविधान के पिता’ के रूप में वर्णित करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने इस नए संविधान को मंजूरी दी और 26 जनवरी 1950 को भारत के नए संविधान के रूप में इसे लागू कर दिया गया।
डॉ. आंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता क्यों कहा जाता है? Dr. Ambedkar As Father Of Indian Constitution
डॉ भीमराव अम्बेडकर एक प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने से पहले उन्होंने लगभग 60 स्वतंत्र और विकसित देशों के संविधानो का अध्ययन किया था जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि । डॉ अम्बेडकर को ‘भारतीय संविधान के निर्माता’ और ‘भारतीय संविधान के पिता’ के रूप में भी जाना जाता है।
भारतीय संविधान के बारे में डॉ अम्बेकर का क्या सोचना था ?
भारतीय संविधान को संविधान सभा को सौपतें हुए डॉ भीमराव अम्बेडकर के शब्द थे “मैं यहां से संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा।
अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे और सविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा। अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय लेना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार से व्यर्थ है।”
डॉ. आंबेडकर के संविधान की सबसे ख़ास बात क्या है ?
ग्रेनविले ऑस्टिन ने डॉ भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान को भारत के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में वर्णित किया। डॉ भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार इस संविधान में भारतीय नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा और गारंटी प्रदान की गई है।
इसके अलावा उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए स्कूलों, कॉलेजों, सिविल सेवाओं व अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
अनुच्छेद 370 के सन्दर्भ में डॉ अम्बेडकर की क्या भूमिका थी ? Dr. Ambedkar’s Role In Article 370
कानून मंत्री के रूप में डॉ भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ( जिसमें जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया गया ) का कड़ा विरोध किया गया था। इस अनुच्छेद को संविधान में उनकी इच्छा के विरुद्ध शामिल किया गया था। हालांकि वे इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे।
डॉ भीमराव अम्बेडकर ने उस समय के कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से कहा था कि “आप चाहते हैं कि भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करें, आपके लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करें, आपके लिए सड़के बनवाए और कश्मीर को भारत का दर्जा मिले।
लेकिन इसके बदले भारत के पास कश्मीर के मामले में कुछ सीमित शक्तियां हो और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार ना हो। इस प्रस्ताव पर सहमति देना भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी। मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में ऐसा कभी नहीं करूंगा। “
बाद में शेख अब्दुल्ला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू से संपर्क किया और अंतत है अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल कर लिया गया।
समान नागरिक संहिता के सन्दर्भ में डॉ अम्बेडकर की क्या भूमिका रही ? Dr. Ambedkar’s Role For Uniform Civil Code Or Hindu Code Bill
डॉ भीमराव अम्बेडकर भारत में एक समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। विधानसभा में बहस के दौरान उन्होंने भारतीय समाज में सुधार करने के उद्देश्य से भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। एक समान नागरिक संहिता, भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। लेकिन उस समय डॉ अम्बेडकर के एक समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव का किसी पार्टी द्वारा समर्थन नहीं किया गया।
डॉ. आंबेडकर ने क़ानून मंत्री के पद से इस्तीफ़ा क्यों दिया ?
बाद में 1951 में ही उन्होंने कानून मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल पर मसौदा सदन में प्रस्तुत किया। जिसमें बाप की विरासत में महिलाओं को अधिकार व विवाह के कानूनों में लैंगिक समानता को शामिल करना आदि प्रावधान थे। लेकिन हिंदू समाज और हिंदू संगठनों द्वारा इस बिल का कड़ा विरोध किया गया।
यहां तक कि कुछ महिला संगठनों द्वारा भी इनका विरोध किया गया। जिन महिलाओं के अधिकारों के लिए वे यह सब कर रहे थे वही उनका विरोध कर रही थी। इस विरोध से दुखी होकर डॉ अम्बेडकर ने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
1952 में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने बॉम्बे नॉर्थ की सीट पर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा लेकिन वे नारायण काजरोलकर से हार गए। बाद में मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और वे अपनी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य करते रहे।
भारत में डॉ अम्बेडकर की सोच पर आधारित अन्य सुधार क्या हुए हैं ?
- डॉ भीमराव अम्बेडकर ने तर्क दिया था कि औद्योगिक और कृषि विकास भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर जोर दिया।
- कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने अपने एक भाषण में कहा था कि डॉ अम्बेडकर के दृष्टिकोण ने सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता की।
- 1923 में उनकी D.Sc थीसिस ‘रुपए की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान’ में उन्होंने रुपए के मूल्य में गिरावट के कारणों की व्याख्या की है।
- डॉ भीमराव अम्बेडकर ने 1951 में भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना की थी, जोकि डॉ अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित था। उन्होंने निम्न आय वर्ग के लिए आयकर का कड़ा विरोध किया था।
- उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने व उसके निरंतर विकास के लिए भूमि राजस्व कर और उत्पाद शुल्क नीतियों में योगदान दिया।
- डॉ भीमराव अम्बेडकर ने भूमि सुधारों और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- डॉ भीमराव अम्बेडकर ने कृषि भूमि का स्वामित्व राज्य के हाथ में होने, राज्य द्वारा उत्पादन के लिए संसाधनों का रखरखाव करने व भारत की आबादी के लिए संसाधनों का उचित वितरण करने पर जोर दिया।
- उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया। जिसे भारत सरकार द्वारा बाद में परिवार नियोजन के रूप में एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया।
- उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए महिलाओं को समान अधिकार देने पर जोर दिया।
- उनके अनुसार कृषि क्षेत्र में काम करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी का कोई उत्पादक उपयोग नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण की वकालत की ताकि इन खेतिहर मजदूरों को औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जा सके। जिसके कारण भारत की आबादी की उत्पादक क्षमता बढ़ाई जा सके।
- भारतीय रिजर्व बैंक, डॉ अम्बेडकर के आइडियाज पर आधारित है, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमिशन, 1926 के सामने प्रस्तुत किए थे।
डॉ भीमराव अम्बेडकर ने दूसरी शादी क्यों की ? Second Marriage Of Dr. BR Ambedkar
एक लंबी बीमारी के कारण 1935 में ही डॉ अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई अम्बेडकर जी का निधन हो गया था। 1940 के दशक में जब डॉ अम्बेडकर संविधान के मसौदे पर काम कर रहे थे, कई शारीरिक बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें नींद ना आने की समस्या का सामना करना पड़ा था, उनके पैरों में भी न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा था। इसके अलावा उन्हें डायबिटीज की भी शिकायत थी, जिसके कारण उन्हें इंसुलिन व होम्योपैथिक दवाई लेनी पड़ती थी।
वे अपना इलाज मुंबई के एक अस्पताल में करवा रहे थे, जहां उनकी मुलाकात एक नर्स शारदा कबीर से हुई। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें समय पर दवाइयां लेने व समय पर खाना खाने की आवश्यकता थी। लेकिन डॉ अम्बेडकर अपने राजनीतिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें इन कार्यों के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। बाद में इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को शारदा कबीर से शादी कर ली।
क्योंकि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए था जो एक अच्छा रसोइया भी हो और उनकी देखभाल के लिए चिकित्सा ज्ञान भी रखता हो। बाद में शारदा कबीर ने सवेत्ता अम्बेडकर का नाम अपना लिया और डॉ अम्बेडकर की मृत्यु तक उनके साथ रही और उनकी देखभाल करती रही।
डॉ भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया ? Dr. Ambedkar & Boudh Dharam
1935 में ही डॉ भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि “मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं।“ उन्होंने हिंदू धर्म को दमनकारी धर्म के रूप में देखा और तभी से किसी अन्य धर्म में परिवर्तन पर विचार करना शुरू कर कर दिया था। डॉ अम्बेडकर ने बचपन से ही हिंदू धर्म की कई बुराइयों को देखा और सहा था। वे अब कोई ऐसा धर्म अपनाना चाहते थे, जिसमें सभी के लिए बंधुता हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में मदद करें।
इसके लिए उन्होंने कई धर्मों को देखा, जाना, उन धर्मों के साहित्य को पढ़ा और उनके प्रमुख व्यक्तियों से भी मिले। लेकिन हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो उनके विचार में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में बाधक था या फिर मनुष्यों के बीच भेदभाव को स्वीकार करता था।
1950 के आसपास उन्होंने बौद्ध धर्म पर ध्यान देना शुरू किया। वह बौद्धों की विश्व फेलोशिप की बैठक में शामिल होने के लिए सीलोन ( आज का श्रीलंका ) भी गए। 1950 में ही उन्होंने पुणे के पास एक नये बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए यह घोषणा की कि “मैं बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहा हूं। जब यह पुस्तक समाप्त हो जाएगी तो मैं बौद्ध धर्म अपना लूंगा।“
1954 में उन्होंने दो बार बर्मा ( आज का म्यांमार ) की यात्रा की। जहाँ दूसरी बार उन्होंने रंगून में होने वाली बौद्ध धर्म की तीसरी विश्व फैलोशिप बैठक में भाग लिया। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1956 में उन्होंने अपनी किताब ‘बुद्ध और उसका धम्म’ का अंतिम कार्य पूरा किया। लेकिन यह किताब उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हो पाई।
अक्टूबर, 1956 में वे श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु हम्मालवा सद्धातिसा से मिले और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। यहां उन्होंने अपने पांच लाख समर्थकों के साथ पारंपरिक तरीके से एक बौद्ध भिक्षु से तीन शरण और पांच उपदेशों को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वहां उपस्थित सभी समर्थकों के साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाऐं भी ली।
1956 में ही डॉ अम्बेडकर दो और किताबों पर भी काम कर रहे थे ‘बुद्ध और कार्ल मार्क्स’ और ‘प्राचीन भारत में क्रांति और प्रति क्रांति’ लेकिन 1956 में ही उनकी मृत्यु के कारण इन दोनों किताबों पर उनका कार्य अधूरा ही रहा।
डॉ भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कैसे हुई ? Dr. Ambekar’s Death Reason
1946 में संविधान का मसौदा तैयार करने के समय से ही उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था जैसे मधुमेह, नींद की कमी, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द आदि। संविधान का मसौदा तैयार करने के दौरान वे अत्यधिक व्यस्त रहते थे, ना तो समय से खाना खा पाते थे और ना ही समय पर सो पाते थे। वो रात को 2 – 3 बजे तक अपना काम करते रहते थे और सुबह भी जल्दी उठ जाया करते थे।
जब थकान और अनियमित खानपान की वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो इसके लिए उन्होंने अत्यधिक दवाइयों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वे दवाइयां खा कर काम करते रहते थे। धीरे-धीरे दवाइयों की अधिकता, थकान और अनियमित दिनचर्या की वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई।
1956 में दवाओं के दुष्परिणाम और आंखों की रोशनी कम होने की वजह से उन्हें जून से अक्टूबर तक बिस्तर पर ही रहना पड़ा। अपना अंतिम साहित्यक कार्य ‘बुद्ध और उसका धम्म’ को समाप्त करने के 3 दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के 26, अलीपुर रोड के उनके घर में नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई।
7 दिसंबर को दादर चौपाटी, मुंबई के समुंदर तट पर एक बौद्ध दाह संस्कार का आयोजन किया गया। लगभग पांच लाख शोक संतप्त लोगों ने उनके दाह संस्कार में भाग लिया। देश के कोने कोने से लाखों शोक संतप्त लोग उनके आखरी दर्शन के लिए पहुंच रहे थे।
16 दिसंबर 1956 को एक धर्म रूपांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि वहां श्मशान में उपस्थित लाखों लोगों को उसी समय बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जा सके। जहां पर डॉ अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार किया गया, उसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है।
डॉ भीमराव अम्बेडकर की विरासत | Dr. Bhimrao Ambedkar’s Legacy
डॉ अम्बेडकर की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर व बेटे यशवंत अम्बेडकर ने डॉ अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए सामाजिक, धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। यशवंत अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध समाज के दूसरे अध्यक्ष के रूप में ( 1957 से 1977 तक ) और ( 1960 से 1966 तक ) महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। यशवंत अम्बेडकर को भैया साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता था।
डॉ अम्बेडकर के बड़े पोते प्रकाश यशवंत अम्बेडकर भारतीय बौद्ध समाज के मुख्य सलाहकार हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं तथा उनके छोटे पुत्र आनंद राज अम्बेडकर रिपब्लिकन सेना का नेतृत्व करते हैं।
डॉ अम्बेडकर की मृत्यु के बाद उनके नोट्स और कागजों में कई अधूरे लेख और हस्तलिखित ड्राफ्ट पाए गए। जिन्हें धीरे-धीरे संकलित करके समय-समय पर प्रकाशित किया गया। इनमें से ही एक ‘वेटिंग फॉर ए वीजा’ उनकी आत्मकथा है जिसे उन्होंने 1935 – 36 के लगभग लिखा था। इसके अलावा द अनटचेबल, द चिल्ड्रन ऑफ इंडियास गेटो आदि भी है।
डॉ भीमराव अम्बेडकर को मिले सम्मान | Dr. Bhimrao Ambedkar’s Achievements
- दिल्ली के उनके पुराने घर 26,अलीपुर रोड पर उनके सम्मान में एक स्मारक बनवाई गई है। जहां पर उनकी कुछ पुरानी वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है।
- उनकी जन्मतिथि 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। जिसे अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में जाना जाता है।
- भारत सरकार द्वारा 1990 में मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हर वर्ष उनके जन्म और मृत्यु की वर्षगांठ पर मुंबई में उनके स्मारक चैत्यभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं।
- भारत में व भारत के बाहर भी कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है जैसे नागपुर में डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जालंधर में डॉ बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और दिल्ली में अम्बेडकर विश्वविद्यालय आदि।
- 1920 में लंदन में जिस घर में वे एक छात्र के रूप में रहते थे, महाराष्ट्र सरकार ने उस घर का अधिग्रहण किया है और इस घर को अम्बेडकर संग्रहालय व सह स्मारक में परिवर्तित करने की घोषणा की है।
- 2012 में हिस्ट्री टीवी 18 और CNN IBN के द्वारा आयोजित एक सर्वे में डॉ अम्बेडकर को बीस लाख वोटों के साथ सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से ऊपर ‘सबसे महानतम भारतीय’ चुना गया था।
- अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एक प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव ने उनका वर्णन अब तक के सर्वोच्च शिक्षित भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में किया।
- अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज विजेता भारत के अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में डॉ अम्बेडकर को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि “डॉ अम्बेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता है। वे देश में अत्यधिक विवादास्पद व्यक्ति हैं, हालांकि यह वास्तविकता नहीं थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अद्भुत है और उन्हें हमेशा के लिए याद किया जाएगा।”
- 2 अप्रैल 1967 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा भारत की संसद में डॉ अम्बेडकर की 12 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था।
- भारतीय डाक द्वारा 1966, 1973, 1991, 2000, 2013 में उनके जन्मदिन को समर्पित डाक टिकट जारी किए गए थे। इसके अलावा 2009, 2015, 2016, 2017 और 2020 में भी अन्य डाक टिकटों पर उन्हें चित्रित किया गया था।
डॉ भीमराव अम्बेडकर के सन्दर्भ में माता रमाबाई की भूमिका क्या थी ?
रमाबाई भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हे रमई या माता रमाबाई के नाम से भी जाना जाता है, डॉ अम्बेडकर की पहली पत्नी थी। इतिहासकारों और लेखकों के अनुसार माता रमाबाई ने डॉ अम्बेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उनकी वास्तविक क्षमता हासिल करने में बहुत सहायता की थी।
माता रमाबाई के वर्णन के बिना डॉ अम्बेडकर जी के बारे में बात करना अधूरा सा लगता है। अगर सच्चे अर्थों में त्याग की देवी की उपाधि किसी को मिलनी चाहिए, तो वह माता रमाबाई ही होंगी। विदेशों में पढ़ाई के दौरान जब डॉ अम्बेडकर अमेरिका और लंदन में उच्च शिक्षा हासिल करने में लगे थे।
उस समय यहां माता रमाबाई अत्यधिक गरीबी और लाचारी में खुद को व बच्चों को पाल रही थी। लेकिन उन्होंने कभी भी बाबासाहेब डॉ अम्बेडकर से इस बारे में शिकायत नहीं की। बाबासाहेब उन्हें प्यार से रामू बुलाते थे और वे उन्हें प्यार से साहेब कहती थी।
डॉ अम्बेडकर और रमाबाई जी के 5 बच्चे थे यशवंत, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरतन ।
अत्यधिक गरीबी और भुखमरी के कारण यशवंत के अलावा अन्य चार बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। जब उनके सबसे छोटे बेटे राजरतन की मृत्यु हुई तो गरीबी के कारण उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसके लिए कफन खरीद पाते। तब माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर दिया था ताकि बच्चे के मृत शरीर को उसमें लपेटा जा सके।
अगर डॉ अम्बेडकर इतना पढ़े-लिखे और गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए कुछ कर पाए तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ माता रमाबाई का भी था। अगर माता रमाबाई ना होती तो शायद डॉ अम्बेडकर यहां तक नहीं पहुंच पाते। माता रमाबाई के जीवन पर कई किताबें लिखी जा चुकी है और कई फिल्में भी बन चुकी हैं। भारत में कई स्थलों का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
डॉ.आंबेडकर जी की बारे में पढ़ना सबके लिए जरुरी क्यों हैं ?
डॉ अम्बेडकर को भारतीय इतिहास में एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया हैं। जातिवाद के मुद्दे पर उनके एकतरफा विचारों के कारण उनकी काफी आलोचना की गई है। लेकिन उनके जैसा राष्ट्रवादी नेता भारत में अब तक दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है।
राष्ट्रवादी होने का दिखावा करने वाले कुछ भ्रष्ट लोगों द्वारा उनके प्रति गलत अवधारणाओं का प्रचार किया गया है। जो लोग यह समझते या मानते हैं कि डॉ अम्बेडकर किसी खास वर्ग विशेष के नेता थे या फिर उन्होंने सिर्फ़ किसी खास वर्ग विशेष के लिए ही कार्य किया है तो यह अवधारणा सरासर गलत है और उन्हें डॉ अम्बेडकर व उनके कार्यों को अच्छी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है।
हालांकि डॉ अम्बेडकर खुद एक अछूत व दलित थे। इसलिए उन्होंने अछूत होने की पीड़ा व दर्द को सहा था। इसलिए उन्होंने भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी और इसके लिए संपूर्ण प्रयास भी किए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अछूतों व दलितों के अधिकारों के लिए ही काम किया। बल्कि सच्चे अर्थों में उन्होंने महिलाओं, किसानों, मजदूरों व देश के सभी नागरिकों के अधिकारों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं।
निष्कर्ष -:
दोस्तों, डॉ अम्बेडकर, जिन्होंने देश के सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए काम किया, जिनका मानना था कि सभी को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे स्वच्छ भोजन, साफ पानी, शिक्षा आदि। ऐसे राष्ट्रवादी नेता को हम नमन करते हैं।
मेरा उन लोगों से विनम्र निवेदन है जो डॉ अम्बेडकर के प्रति गलत अवधारणा लिए बैठे हैं। पहले वे डॉ अम्बेडकर के बारे में गहनता से पढ़े और फिर निर्णय लें की वे किन मायनों में सही या गलत है।
इनके बारे में भी पढ़े -:
- रितेश अग्रवाल की जीवनी | Ritesh Agarwal Biography In Hindi
- राकेश झुनझुनवाला की जीवनी। Rakesh Jhunjhunwala Biography In Hindi
- वारेन बफ़ेट की प्रेरणादायक जीवनी | Warren Buffett Biography In Hindi
हम उम्मीद करते हैं की आपको यह ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मोटिवेशनल जानकारी लाते रहे। इसके अलावा आप इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
ताकि जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन जीवन की परेशानियों के कारण, उन्होंने हार मान ली है। तो वे लोग इस ब्लॉग ‘Dr. Br Ambedkar Biography In Hindi‘ से प्रेरित हो सकें।
इसी तरह की और मोटिवेशनल जानकारी के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो करें।
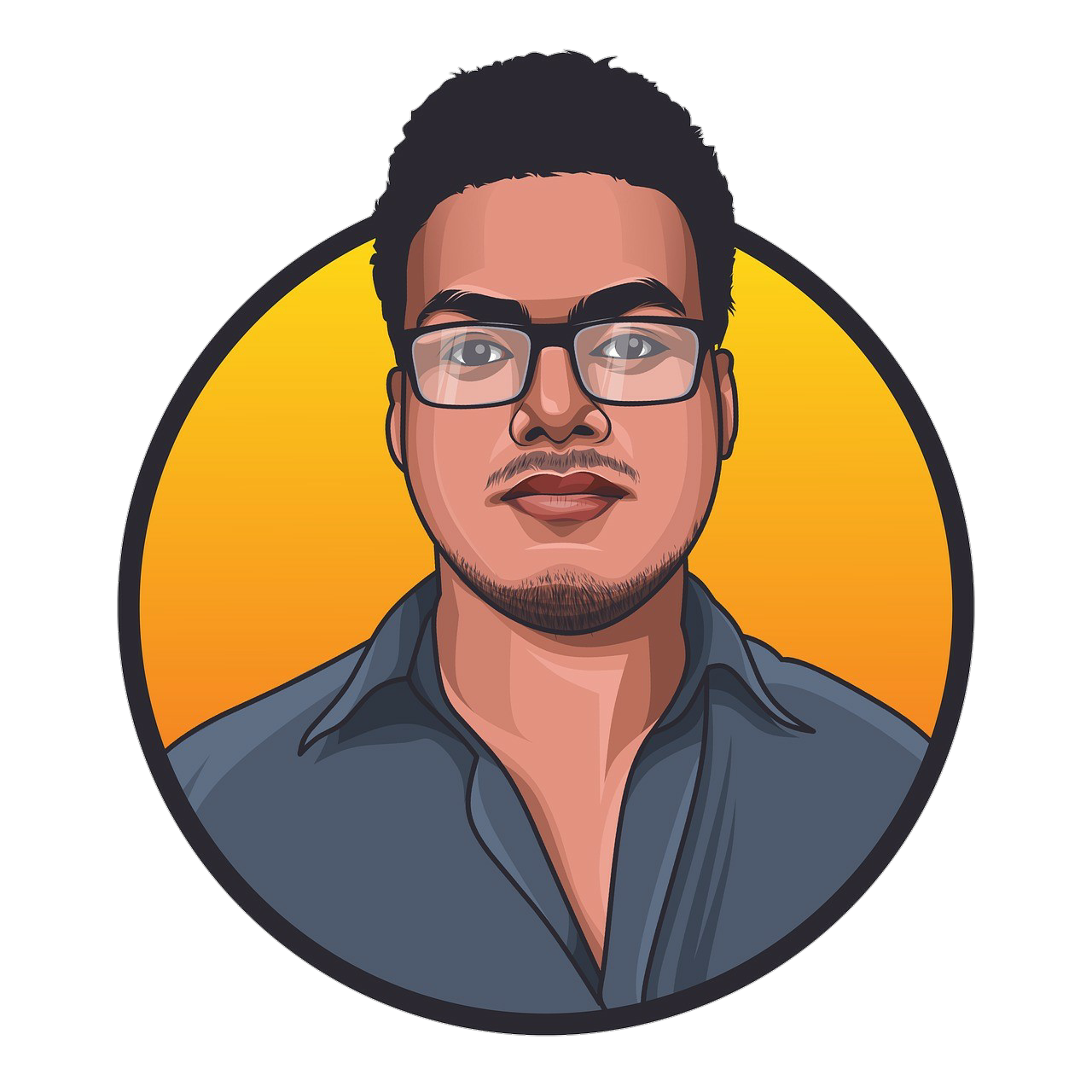


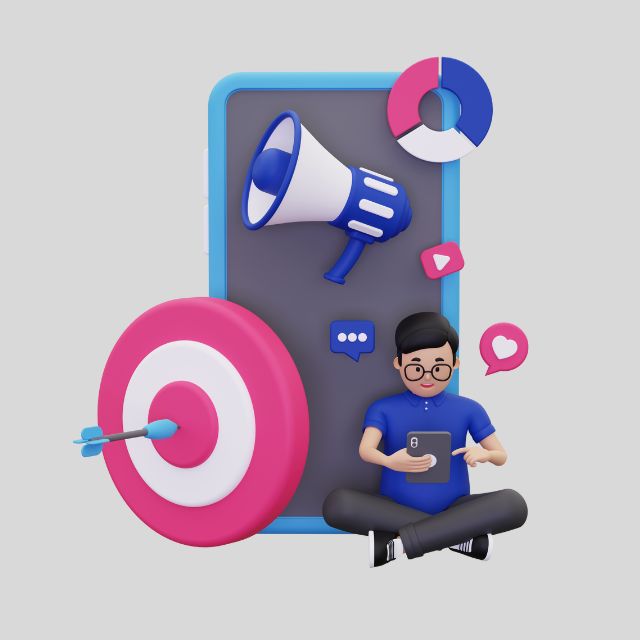



Leave a Reply